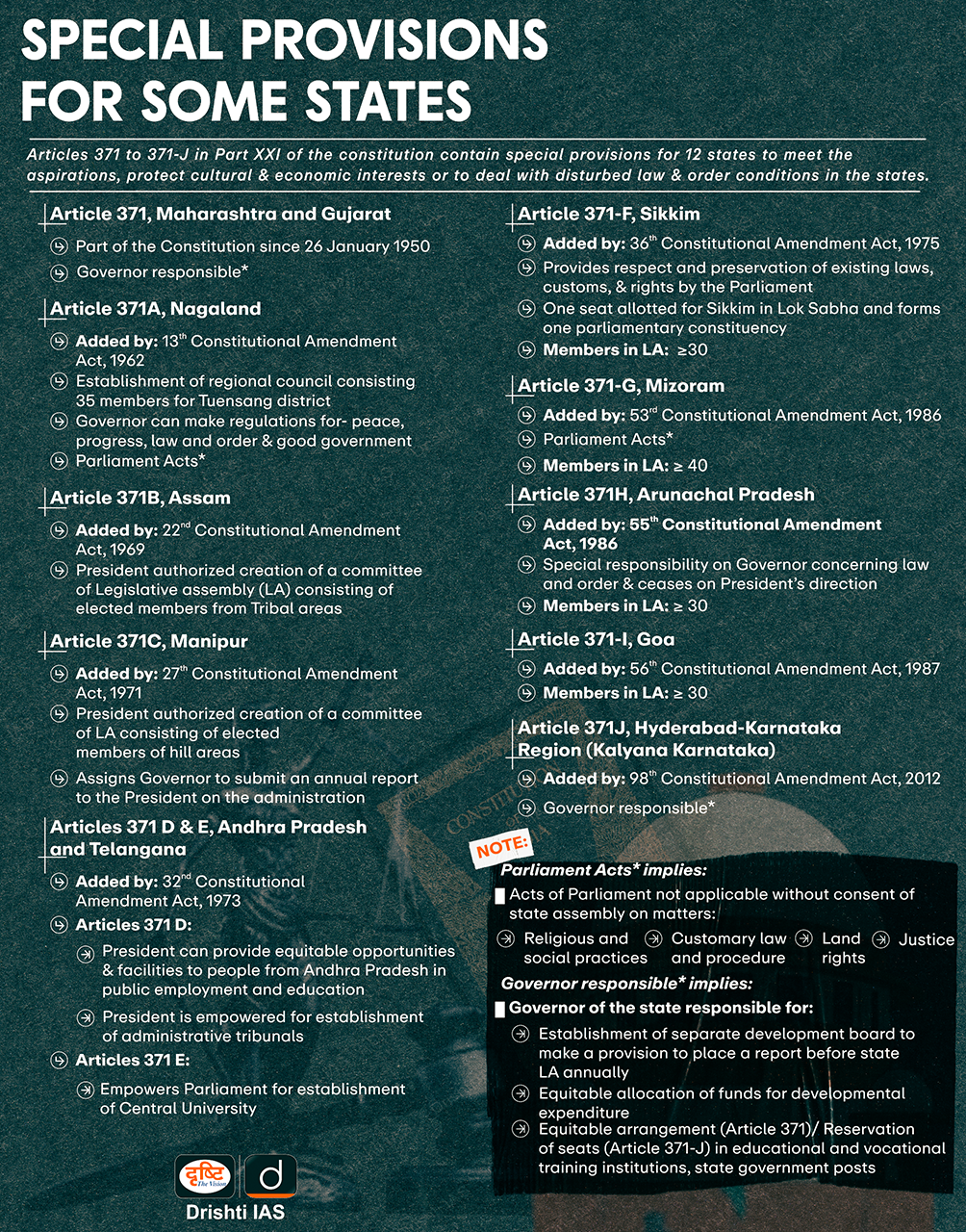होम / एडिटोरियल
सांविधानिक विधि
विशेष श्रेणी का दर्जा
« »13-Jun-2024
स्रोत: द हिंदू
परिचय
बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को रेखांकित किया है, यह एक ऐसा दर्जा है जिसमें केंद्र सरकार, दर्जा प्राप्त राज्य को वित्तीय सहायता बढ़ाने का वादा करती है। इस दर्जे के पक्ष में राज्य सरकार का प्रस्ताव इस की आवश्यकता को और भी बढ़ा देता है। SCS वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिये बढ़ी हुई केंद्रीय निधि और कर लाभ जैसे विशेष सहायता प्रदान करता है। हालाँकि, इसके आवंटन के विषय में चर्चा, विशेष रूप से SCS के लिये बिहार के प्रयास के विषय में, भारत के संघीय ढाँचे के भीतर विधिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।
SCS का विधिक ढाँचा और ऐतिहासिक पूर्वनिर्णय क्या हैं?
- पाँचवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर वर्ष 1969 में तैयार की गई SCS एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करना है।
- SCS केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में सहायता करता है।
- केंद्रीय वित्तपोषण और कर अनुदानों के संदर्भ में अधिमान्य उपचार के माध्यम से, SCS का उद्देश्य इन क्षेत्रों का उत्थान करना तथा उनके अधिक विकसित समकक्षों के साथ अंतर को कम करना है।
- पात्रता के मानदंड में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं-
- पहाड़ी क्षेत्र;
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा भाग;
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान;
- आर्थिक एवं अवसंरचना पिछड़ापन; तथा
- राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।
- भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 275, केंद्र सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं को दरकिनार करते हुए किसी भी राज्य को अनुपूरक वित्तीय सहायता देने का अधिकार देता है।
SCS से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
SCS के क्या लाभ हैं?
- अतीत में, SCS राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर लगभग 30% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती थी।
- 14वें और 15वें वित्त आयोगों की अनुशंसाओं तथा योजना आयोग के विघटन के फलस्वरूप, SCS राज्यों को दी जाने वाली यह सहायता सभी राज्यों के लिये विभाज्य कुल निधियों के बढ़े हुए हस्तांतरण में सम्मिलित कर दी गई है (15वें वित्त आयोग में इसे 32% से बढ़ाकर 41% कर दिया गया है)।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% भाग केंद्र SCS राज्यों को देता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह 60% या 75% है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराती हैं।
- यदि किसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली धनराशि समाप्त नहीं होती तो उसे आगामी वर्ष में ले जाया जाता है।
- इन राज्यों को उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में महत्त्वपूर्ण अनुदान प्रदान किये जाते हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30%, विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है।
SCS के संबंध में महत्त्वपूर्ण चिंताएँ क्या हैं?
- 14वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित आधारों पर विशेष राज्य का दर्जा जारी रखने का विरोध किया था।
- SCS वाले राज्यों को अतिरिक्त धनराशि, कर अनुदानों एवं अन्य लाभों का प्रावधान, केंद्र सरकार के बजट पर महत्त्वपूर्ण वित्तीय भार डालता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता के विषय में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- कुछ राज्यों को विशेष राज्य का आवंटन तथा अन्य को इससे वंचित रखने से संसाधनों का असमान वितरण हो सकता है, जिससे निष्पक्षता और समानता पर प्रश्न उठ सकते हैं।
- ऐसी आशंकाएँ हैं कि SCS राज्य केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे स्वतंत्र रूप से राजस्व उत्पन्न करने की उनकी प्रेरणा कम हो जाएगी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न होगी।
- मूल रूप से अस्थायी दर्जा प्राप्त राज्यों द्वारा SCS का निरंतर उपयोग, आवधिक पुनर्मूल्यांकन या प्रभाव मूल्यांकन के बिना इस पदनाम के स्थायी रूप से जारी रहने के विषय में चिंता उत्पन्न करता है।
- SCS के लिये स्पष्ट संवैधानिक या विधिक आधार का अभाव इसे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाता है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्र सरकार जैसे निकायों के प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिनमें मज़बूत विधि ढाँचे का अभाव होता है।
क्या अन्य राज्य भी SCS चाहते हैं?
|
कौन-सी आर्थिक चुनौतियों के कारण बिहार को SCS की मांग करनी पड़ी?
- बिहार में SCS दर्जे की माँग के लिये विशिष्ट आर्थिक चुनौतियाँ उत्तरदायी हैं, जिनमें प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से काफी कम होना तथा मानव विकास संकेतकों में स्पष्ट कमियाँ शामिल हैं।
- राज्य की राजकोषीय स्थिति इसके विभाजन के दुष्परिणामों, उद्योगों के झारखंड की ओर पलायन, सिंचाई के लिये पानी की कमी और बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण और भी जटिल हो गई है।
- जाति-आधारित सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्ष बिहार में गरीबी की व्यापकता को रेखांकित करते हैं तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिये लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं।
- बिहार की SCS की मांग के पीछे महत्त्वपूर्ण आर्थिक अनिवार्यताएँ होने के बावजूद, केंद्र की एक के बाद एक सरकारें वित्तीय बाधाओं और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इसे स्वीकार करने में हिचकिचाती रही हैं।
- विशेष राज्य के दर्जे के लिये बिहार की याचिका का विधिक आधार, वित्तीय संघवाद और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर आधारित है, जो चल रही बहस में एक सूक्ष्म स्तर जोड़ता है।
क्या बिहार SCS अनुदान के लिये मानदंडों को पूरा करता है?
- यद्यपि बिहार SCS का दर्जा प्राप्त करने के लिये अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन यह पहाड़ी क्षेत्रों और भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जिसे बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है।
- वर्ष 2013 में, केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को “सबसे कम विकसित श्रेणी” में रखा और SCS के बजाय धन हस्तांतरित करने के लिये ‘बहु-आयामी सूचकांक’ पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिस पर राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पुनर्विचार किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
बिहार की SCS की मांग पर बहस, भारत के संघीय ढाँचे के भीतर विधिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के बीच जटिल अंतर्विरोध को दर्शाती है। चूँकि नीति निर्माता इस मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें इतिहास के सबक और वर्तमान की अनिवार्यताओं पर ध्यान देना चाहिये तथा एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करना चाहिये जो राजकोषीय संघवाद तथा वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा दे। अंततः बिहार की विशेष दर्जा प्राप्ति की अभिलाषा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने एवं पूरे देश में समान विकास को बढ़ावा देने की व्यापक अनिवार्यता को रेखांकित करती है। इस बहस के विधिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को विवेक तथा दूरदर्शिता के साथ समझकर, नीति निर्माता सभी के लिये अधिक समृद्ध एवं समान भविष्य की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं।