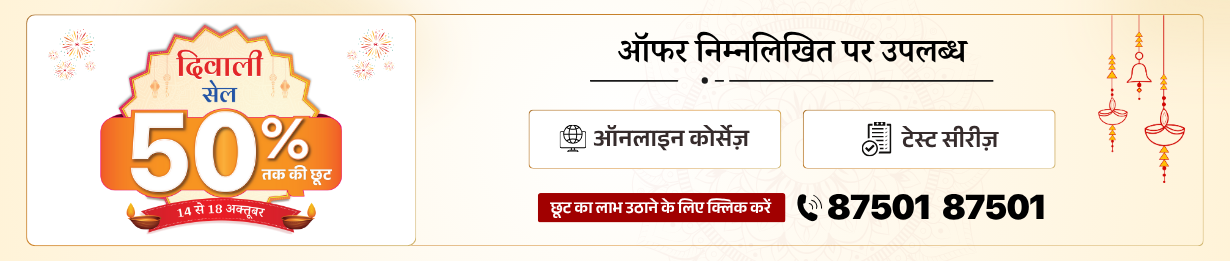करेंट अफेयर्स और संग्रह
होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह
सिविल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11
17-Oct-2025
|
करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह और अन्य "तत्संबंधी वादपत्र के नामंजूर करने पर विचार करते समय, केवल वादपत्र में दिये गए कथनों पर ही विचार किया जाना है, अन्य किसी बात पर नहीं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वाद विधि द्वारा वर्जित है या नहीं। इस स्तर पर, बचाव पक्ष पर विचार नहीं किया जाना है। इस प्रकार, वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, इसका अवधारण वादपत्र में दिये गए कथनों के आधार पर किया जाना है।" न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 के अधीन किसी वादपत्र का नामंजूर करना केवल वादपत्र के कथनों पर आधारित होना चाहिये, प्रतिवादी की प्रतिरक्षा या बाहरी साक्ष्य पर विचार किये बिना। पीठ ने इस बात पर बल दिया कि कोई वाद विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, इसका अवधारण केवल वादपत्र से ही होना चाहिये, न कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तथ्यों से।
- उच्चतम न्यायालय ने करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह एवं अन्य (2025) की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- अपीलकर्त्ता ने दिलबाग सिंह के साथ मिलकर एक सिविल वाद दायर किया, जिसमें कृषि भूमि पर स्वामित्व की घोषणा, उस पर कब्जा, अंत:कालीन लाभ और प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी व्यादेश की मांग की गई।
- इस भूमि के मूल स्वामी रौनक सिंह उर्फ रौनाकी थे, जिनकी 5 अक्टूबर 1924 को बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी, तथा वे अपने पीछे विधवा करतार कौर को छोड़ गए थे।
- करतार कौर और चिंकी व निक्की, जो रौनक सिंह की बहनें और वादी पक्ष की हित-पूर्ववर्ती थीं, के बीच उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हुआ।
- उत्तराधिकार विवाद के लंबित रहने के दौरान, करतार कौर ने कथित तौर पर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में हरचंद नामक व्यक्ति के पक्ष में एक दान विलेख निष्पादित किया।
- रौनक सिंह की बहनों ने सिविल न्यायालय में दान विलेख की वैधता को चुनौती दी।
- 22 मार्च 1935 को सिविल न्यायालय ने इस आधार पर दान विलेख को अवैध घोषित कर दिया कि करतार कौर के पास संपत्ति पर केवल सीमित अधिकार थे।
- 11 सितंबर 1975 के आदेश द्वारा दान विलेख को अपास्त कर दिया गया तथा करतार कौर को विवादित भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया।
- इस आदेश के परिणामस्वरूप, 13 मई 1976 को करतार कौर के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया।
- नामांतरण की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान 28 दिसंबर 1983 को करतार कौर की मृत्यु हो गई।
- उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादियों ने 15 दिसंबर 1976 की एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत प्रस्तुत की, जिसे कथित तौर पर करतार कौर ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था, और उसके आधार पर नामांतरण का दावा किया।
- 29 अप्रैल 1984 के आदेश द्वारा राजस्व प्राधिकारियों ने प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर रौनक सिंह की बहन के विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में नामांतरण का आदेश दिया, तथा वसीयत के आधार पर प्रतिवादियों के दावे को खारिज कर दिया।
- प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को कलेक्टर ने 15 अप्रैल 1985 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।
- प्रतिवादियों ने मुकदमेबाजी के लगातार दौर के माध्यम से नामांतरण मामले को उच्च न्यायालयों तक पहुँचाया।
- नामांतरण की कार्यवाही से उत्पन्न मुकदमेबाजी अंततः 20 जुलाई 2017 को वादी के विरुद्ध समाप्त हो गई।
- तत्पश्चात्, वादियों ने 31 मई 2019 को वर्तमान में वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने स्वयं को रौनक सिंह की बहनों के माध्यम से करतार कौर का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने का दावा किया।
- वादियों ने 15 दिसंबर 1976 की वसीयत को अकृत और शून्य और कपटपूर्ण कृत्य बताते हुए चुनौती दी तथा अपने स्वामित्व की घोषणा की मांग की।
- प्रतिवादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11(घ) के अधीन एक आवेदन दायर किया, जिसमें इस आधार पर वादपत्र को नामंजूर करने की मांग की गई कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि चूँकि वसीयत 1983 में बनाई गई थी और वादियों को नामांतरण की कार्यवाही के दौरान इसके अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिये वसीयत को चुनौती देने वाली घोषणा के लिये वाद दायर करने पर तीन वर्ष की परिसीमा के कारण वर्जित था।
- प्रतिवादियों ने वादी संख्या 1 के पिता द्वारा दायर सिविल वाद संख्या 648/2012 के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का भी आरोप लगाया, जिसमें वसीयत को चुनौती दिये बिना ही नामांतरण आदेश को चुनौती दी गई थी, और वादपत्र को 17 मई 2013 के आदेश के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन नामंजूर कर दिया गया था।
- प्रतिवादियों ने दावा किया कि वर्तमान वाद पूर्ववर्ती वाद के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 द्वारा वर्जित है।
- विचारण न्यायालय ने 7 जनवरी 2020 के आदेश के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन प्रतिवादियों के आवेदन को नामंजूर कर दिया, जिसमें कहा गया कि वाद पूर्व दृष्टया परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था और परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न था।
- इससे व्यथित होकर प्रतिवादियों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की।
- उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी 2022 के एकपक्षीय आदेश के अधीन पुनरीक्षण को अनुमति दे दी और वाद को नामंजूर कर दिया।
- वादी द्वारा दायर रिकॉल आवेदन को 4 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11(घ) के अधीन किसी वादपत्र को नामंजूर करने पर विचार करते समय, केवल वादपत्र में दिये गए कथनों पर विचार किया जाना चाहिये जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, और इस स्तर पर प्रतिपक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि न वादपत्र और न ही अभिलेख में विद्यमान किसी दस्तावेज़ से यह संकेत मिलता है कि करतार कौर द्वारा कथित रूप से निष्पादित वसीयत की जांच की गई थी या इसकी वैधता का परीक्षण किया गया था और नियमित सिविल कार्यवाही में इसे बरकरार रखा गया था।
- नामांतरण प्रविष्टियाँ स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं तथा इनका उद्देश्य केवल उस व्यक्ति से कर वसूलना होता है जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
- वादपत्र में यह दर्शाया गया है कि नामांतरण की कार्यवाही 2017 में पूरी हो गई थी और उसके तीन वर्ष के भीतर वाद संस्थित कर दिया गया था।
- यह वाद केवल वसीयत को अकृत और शून्य घोषित करने के लिये नहीं था, अपितु स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिये भी था।
- जहाँ कोई वाद स्वामित्व के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे के लिये है, वहाँ परिसीमा काल बारह वर्ष है, जब प्रतिवादियों का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है, जैसा कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार है।
- प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना स्वामित्व पूर्ण किया है या नहीं, यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और इसका समाधान केवल साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के बाद ही किया जा सकता है, तथा इसे वादपत्र को प्रारंभ में ही नामंजूर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
- जहाँ किसी वाद में कई अनुतोष मांगे जाते हैं, यदि उनमें से कोई भी परिसीमा काल के भीतर है, तो वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(घ) के अधीन विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामंजूर नहीं किया जा सकता है।
- यद्यपि स्वामित्व की घोषणा के लिये वाद दायर करने की परिसीमा तीन वर्ष है, किंतु स्वामित्व के आधार पर कब्जे की वसूली के लिये परिसीमा उस तिथि से बारह वर्ष है, जिस तिथि से कब्जा प्रतिकूल हो जाता है।
- चूँकि हितबद्ध पूर्ववर्ती द्वारा दायर प्रथम वाद का विचारण नहीं हुआ था और वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन नामंजूर कर दिया गया था, इसलिये उचित अनुतोष के साथ एक नया वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित नहीं किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय ने वादपत्र के कथनों पर समग्रता से विचार नहीं किया तथा केवल इस तथ्य से प्रभावित हुआ कि वसीयत छत्तीस वर्ष पुरानी थी, तथा इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वसीयत की वैधता पर नामांतरण कार्यवाही के दौरान प्रश्न उठाए गए थे, जिसका निपटारा 2017 में हुआ था।
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया, तथा विचारण न्यायालय को वाद को आगे बढ़ाने का निदेश दिया तथा स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को विवाद्यकों के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं लिया जाएगा।
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 - वादपत्र की नामंजूरी क्या है?
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 में इसके अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में वादपत्र को नामंजूर करने का उपबंध है।
- खण्ड (क) के अनुसार, जहाँ वाद-हेतुक प्रकट नहीं गया है, वहाँ वादपत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा।
- खण्ड (ख) में उन मामलों में नामंजूरी का उपबंध है, जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
- खण्ड (ग) उन मामलों से संबंधित है जहाँअनुतोष राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, किंतु वादपत्र पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं लगा है, और वादी विहित समय के भीतर अपेक्षित स्टाम्प-पेपर उपलब्ध कराने में असफल रहता है।
- खण्ड (घ) के अनुसार, जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
- खण्ड (ङ) में उस स्थिति में नामंजूरी का उपबंध है, जब वादपत्र दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया हो।
- खण्ड (च) में उस स्थिति में नामंजूरी का उपबंध है, जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।
- परंतुक में यह उपबंध है कि मूल्यांकन की शुद्धि के लिये या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टांप-पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किये जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।
- आदेश 7 नियम 11 के अधीन किसी वादपत्र को नामंजूर करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिये।
- खण्ड (घ) के अंतर्गत न्यायालय को वादपत्र में दिये गए कथनों से ही यह अवधारित करना होगा कि क्या वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, जिसमें परिसीमा विधि भी सम्मिलित है।
- आदेश 7 नियम 11(घ) के अधीन जांच का दायरा वाद्प्त्र और उसके साथ संलग्न या उसमें संदर्भित दस्तावेज़ों तक सीमित है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन पर निर्णय करते समय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता।
- इस शक्ति का प्रयोग केवल स्पष्ट और प्रत्यक्ष मामलों में ही किया जाना चाहिये, जहाँ वादपत्र पूर्वदृष्टया वर्जित हो।
- जहाँ परिसीमा अवधारण के लिये साक्ष्य की जांच या विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों पर विचार की आवश्यकता होती है, वहाँ वादपत्र को खण्ड (घ) के अधीन नामंजूर नहीं किया जा सकता।
- आदेश 7 नियम 11 के अधीन नामंजूरी के लिये आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय वादपत्र की चारदीवारी से आगे नहीं जा सकता।
- जहाँ कई अनुतोषों का दावा किया गया हो और यहाँ तक कि एक अनुतोष भी परिसीमा के भीतर हो, तो वादपत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण पूरी तरह से नामंजूर नहीं किया जा सकता।
- इस उपबंध का उपयोग केवल तकनीकी आधार पर, योग्यता के आधार पर पूर्ण निर्णय लिये बिना, वास्तविक दावों को खारिज करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
सिविल कानून
सूचना का अधिकार अधिनियम और वस्तु एवं सेवा कर सूचना का प्रकटीकरण
17-Oct-2025
|
आदर्श गौतम पिम्पारे बनाम महाराष्ट्र राज्य “बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह अभिप्रेत किया कि जीएसटी रिटर्न पर- पक्षकार सूचना के रूप में अभिहित होती है, जिसके प्रकटीकरण के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अंतर्गत अनिवार्य नोटिस दिया जाना आवश्यक है। साथ ही, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण को प्रतिषेध करती है, जब तक कि विधि द्वारा निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में उसकी अनुमति न दी गई हो।” न्यायमूर्ति अरुण आर. पेडनेकर |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति अरुण आर. पेडनेकर ने आदर्श गौतम पिंपरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के अधीन GST रिटर्न की जानकारी देने से इंकार करने को बरकरार रखा और निर्णय दिया कि ऐसी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अधीन पर-पक्षार की गोपनीय जानकारी के रूप में और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के अधीन सांविधिक रूप से प्रतिषिद्ध प्रकटीकरण के रूप में संरक्षित है।
आदर्श गौतम पिंपरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता आदर्श गौतम पिंपरे ने 13.02.2023 को जनहित अधिकारी/सहायक राज्य कर आयुक्त के समक्ष RTI आवेदन दायर कर उदगीर, जिला लातूर के छह विभिन्न उद्योगों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008 से 2023 तक GST प्रस्तुत करने के संबंध में जानकारी मांगी थी।
- ये छह उद्योग थे: मेसर्स व्यंकटेश्वर महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, मेसर्स अनिकेत ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स मयूरेश्वर ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स न्यू प्रसाद प्रोडक्ट्स एंड एजेंसीज़, मेसर्स कल्याणी ट्रेडिंग और मेसर्स प्रसाद इंडस्ट्रीज।
- सूचना अधिकारी ने संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आवेदन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।
- संबंधित उद्योगों ने याचिकाकर्त्ता को सूचना उपलब्ध कराने पर आपत्ति जताई।
- उद्योगों की आपत्तियों के आधार पर सूचना अधिकारी ने याचिकाकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।
- याचिकाकर्त्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप राज्य कर आयुक्त के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपील दायर की, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि फर्मों ने पर-पक्षकार को सूचना प्रदान करने के लिये सहमति देने से इंकार कर दिया था।
- तत्पश्चात् याचिकाकर्त्ता ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष धारा 19(3) के अधीन द्वितीय अपील दायर की, जिसे निचले प्राधिकारियों के आदेशों को बरकरार रखते हुए दिनांक 30.12.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
- याचिकाकर्त्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से तीनों आदेशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि छह फर्मों ने दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके और GST जमा नहीं करके सरकारी निविदाएँ हासिल की थीं, जिससे जनता के पैसे के साथ भारी कपट हुआ था, और इस शिकायत को प्रमाणित करने के लिये जानकारी की आवश्यकता थी।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि GST रिटर्न लोक दस्तावेज़ हैं, न कि व्यक्तिगत या पर-पक्षकार की जानकारी जिसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अधीन सहमति की आवश्यकता होती है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
पर-पक्षकार को अनिवार्य सूचना पर:
- न्यायालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत के उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2020) में संविधान पीठ के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें कहा गया था कि जब सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के अधीन व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो धारा 11 के अधीन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि पर-व्यक्ति को सूचना को प्रथम दृष्टया गोपनीय माना जाना चाहिये, तथा प्रभावित पक्षकारों को धारा 11 के अधीन प्रकटीकरण का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिये। धारा 8 और धारा 11 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये, तथा प्रकटीकरण की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिये जब लोकहित संभावित नुकसान से अधिक हो।
- न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि उद्योगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिये था, तथा कहा कि सूचना अधिकारी ने धारा 11 के अधीन अनिवार्य प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया है।
संरक्षित सूचना के रूप में GST रिटर्न पर:
- न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 का विश्लेषण किया, जो विशेष रूप से उपधारा (3) में दिये गए उपबंध के सिवाय GST रिटर्न, विवरण और दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है।
- न्यायालय ने यह सिद्धांत लागू किया कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एक विशेष और बाद में पारित अधिनियम होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम (एक सामान्य अधिनियम) पर अधिभावी होगा। इसलिये, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के अधीन प्रतिषिद्ध जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रकट नहीं की जा सकती।
जनहित अपवाद पर:
- न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता का बड़े पैमाने पर कपट का आरोप पूरी तरह से निराधार था और उसके लिये प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं था। प्राधिकारियों ने सही ढंग से अवधारित किया कि इसमें कोई व्यापक जनहित शामिल नहीं था जो धारा 8(1)(ञ) के उपबंध के अधीन प्रकटीकरण को उचित ठहराता हो।
अंतिम निर्णय:
- न्यायालय ने जनहित अधिकारी/सहायक राज्य कर आयुक्त, प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप राज्य कर आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित सभी तीन आदेशों को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।
सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?
बारे में:
- यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, भारत का कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकारी से सूचना का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर देना आवश्यक है।
- सूचना का अधिकार विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ ।
उद्देश्य:
- नागरिकों को सशक्त बनाना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- भ्रष्टाचार से निपटने के लिये।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:
- इसमें उपबंधित किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त (केंद्र और राज्य दोनों के) केंद्र सरकार द्वारा विहित अवधि तक पद धारण करेंगे। इस संशोधन से पहले, उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था।
- इसमें उपबंधित किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्र तथा राज्य के) के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन महत्त्वपूर्ण उपबंध:
- सूचना का अधिकार (धारा 3):
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है।
- लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं (धारा 4):
- अभिलेखों का रखरखाव एवं सूचीकरण करना।
- उचित समय के भीतर अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करें।
- अधिनियमन के 120 दिनों के भीतर संगठन के बारे में विभिन्न विवरण प्रकाशित करें।
- प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण पदान करे।
- लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम (धारा 5):
- प्रत्येक लोक प्राधिकारी को केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- उप-मंडल या उप-जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे।
- सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध (धारा 6):
- अनुरोध लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक रूप से किया जा सकता है।
- आवेदकों को सूचना मांगने के लिये कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
- अनुरोध का निपटारा (धारा 7):
- अनुरोध के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- जानकारी उपलब्ध कराने के लिये शुल्क लिया जा सकता है।
- सूचना के प्रकट किये जाने से छूट (धारा 8):
- इसमें छूट के लिये विभिन्न आधारों की सूची दी गई है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी सम्मिलित हैं।
- छूट के होते हुए भी लोक हित में प्रकटीकरण संभव है।
- कतिपय मामलों में पहुँच के लिये अस्वीकृति के आधार (धारा 9):
- यदि अनुरोध कॉपीराइट का उल्लंघन करता हो तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
- पृथक्करणीयता (धारा 10):
- यदि छूट प्राप्त सूचना को उचित रूप से अलग किया जा सकता है तो अभिलेख के किसी भाग तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
- पर-व्यक्ति सूचना (धारा 11):
- किसी पर-व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना को संभालने की प्रक्रिया।
- सूचना आयोगों का गठन (धारा 12-15):
- केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की स्थापना।
- सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया।
- पदावधि एवं सेवा शर्ते (धारा 13 एवं 16):
- सूचना आयुक्तों के लिये सेवा की शर्तों, वेतन और शर्तों का विवरण।
- सूचना आयुक्तों को हटाना (धारा 14 और 17):
- सूचना आयुक्तों को हटाने के आधार और प्रक्रिया का उल्लेख।
- सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य (धारा 18):
- आयोग परिवादों की जांच कर सकता है और उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं।
- अपील प्रक्रिया (धारा 19):
- प्रथम और द्वितीय अपील प्रक्रियाओं से संबंधित है।
- सूचना आयोगों के निर्णय बाध्यकारी हैं।
- शास्ति (धारा 20):
- अनुचित इंकार, विलंब या बाधा के लिये लोक सूचना अधिकारियों के लिये शास्ति।
- निरतंर उल्लंघन के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।
पारिवारिक कानून
यदि पुत्र जीवित है तो पुत्री 1956 से पूर्व की मिताक्षरा संपत्ति की हकदार नहीं है
17-Oct-2025
|
श्रीमती रागमानिया (मृत) एल.आर.एस .बनाम जगमेत एवं अन्य "यह विधि का सुव्यवस्थित एवं स्थापित सिद्धांत है कि मिताक्षरा विधि के अनुसार, अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन से पूर्व पुत्री अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं करती थी। मिताक्षरा विधि के अधीन, किसी पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति भी केवल उसकी पुरुष संतान पर ही अवलंबित होती थी, तथा ऐसी पुरुष संतान के अभाव में ही वह अन्य उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित होती थी। उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार, किसी पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति उसके पुरुष उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त होती थी, और केवल ऐसी संतान के अभाव में वह अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाती थी।" न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास |
स्रोत: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने यह अभिप्रेत किया कि मिताक्षरा विधि के अधीन, यदि किसी हिंदू पिता की मृत्यु वर्ष 1956 से पूर्व हो गई हो, तो उसकी पुत्री उस संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होगी, यदि उसका कोई पुत्र जीवित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में पुत्री संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है, परंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्ष 2005 द्वारा किया गया संशोधन, 1956 से पूर्व की उत्तराधिकार संबंधी स्थितियों पर भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होगा।
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रागमानिया (मृत) थ्रू एल.आर.एस. बनाम जगमेत एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
श्रीमती रागमानिया (मृत) बनाम जगमेत एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- अपीलकर्त्ता श्रीमती रागमनिया बैगादास की बहन थीं, दोनों सुधीनराम की संतान थी।
- रागमानिया की मृत्यु के पश्चात्, उनके विधिक उत्तराधिकारी करीमन दास को अपीलकर्त्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।
- प्रत्यर्थियों में जगमेत (बैगादास का पुत्र), बुधियारो (बैगादास की विधवा) और छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित थे।
- परिवार हिंदू धर्म का पालन करता था और हिंदू विधि द्वारा शासित था।
- विवादित संपत्ति में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पुहपुत्रा गाँव की कृषि भूमि सम्मिलित थी।
- शुरुआत में यह जमीन सुधीनराम और उनके भाई बुधौ के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज थी।
- सुधीनराम की मृत्यु लगभग 1950-51 में हो गई थी, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमित होने से पहले की बात है।
- सुधीनराम की मृत्यु के समय अपीलकर्त्ता की आयु लगभग 10 वर्ष थी।
- सुधीनराम की मृत्यु के पश्चात्, बैगादास को संपूर्ण संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो गया।
- बैगादास ने राजस्व अभिलेखों में अपना नामांतरण करा लिया।
- अपीलार्थी का विवाह बैगादास द्वारा उनके पिता की मृत्यु के बाद तय किया गया था।
- बैगादास ने अपनी पुत्री जगमीत के पक्ष में संपत्ति के नामांतरण के लिये नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन दायर किया।
- अपीलकर्त्ता को समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से म्यू नामांतरण टेशन आवेदन के बारे में पता चला।
- अपीलकर्त्ता ने राजस्व वाद संख्या 13-ए-27/2002-03 में आपत्तियाँ दायर कीं, तथा अपने उचित अंश का दावा किया।
- बैगादास ने स्वीकार किया कि अपीलकर्त्ता उसकी बहन है, परंतु तर्क दिया कि विवाह के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता।
- तहसीलदार ने 23 अगस्त 2003 को अपीलकर्त्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया।
- अपीलकर्त्ता ने 6 अक्टूबर 2005 को सिविल वाद संख्या 181-A/2005 दायर किया जिसमें स्वामित्व और विभाजन की घोषणा की मांग की गई।
- प्रत्यर्थियों ने दलील दी कि सुधीनराम की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले 1950-51 में हो गई थी।
- प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि उत्तराधिकार पुरानी मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होगा।
- प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि मिताक्षरा विधि के अधीन, जब तक पुरुष उत्तराधिकारी जीवित है, विवाहित पुत्री को कोई अधिकार नहीं है।
- अपीलकर्त्ता ने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि सुधीनराम की मृत्यु कब हुई।
- साक्षी PW-3 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि सुधीन की मृत्यु 17 अक्टूबर 2008 से 60 वर्ष पहले हो गई थी।
- इस स्वीकृति से यह स्थापित हो गया कि सुधीन की मृत्यु 1948-49 के आसपास हुई थी।
- विचरण न्यायालय ने 26 दिसंबर 2008 के निर्णय के अधीन वाद खारिज कर दिया।
- विचरण न्यायालय ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता क्योंकि मृत्यु 1956 से पहले हो गई थी।
- प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 23 जनवरी 2014 को निर्णय की पुष्टि की।
- अपीलकर्त्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 178/2014 दायर की।
- अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि निचले न्यायालयों ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन की अनदेखी की है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने माना कि चूँकि वादी सुधीन की मृत्यु के समय अभिवचन देने में असफल रहा तथा उसने प्रतिवादी के इस विशिष्ट अभिवचन का खंडन नहीं किया कि मृत्यु 1950-51 में हुई थी, तथा साथ ही PW-3 ने स्वीकार किया कि सुधीन की मृत्यु 2008 से 60 वर्ष पूर्व हो गई थी, इसलिये यह निश्चायक रूप से स्थापित हो गया कि सुधीन की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व, 1948-49 के आसपास हुई थी।
- न्यायालय ने कहा कि चूँकि सुधीन की मृत्यु 1956 से पहले हो गई थी, इसलिये उत्तराधिकार पुराने हिंदू विधि के अधीन शुरू हुआ और पक्षकार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होंगे, जिससे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और इसका 2005 का संशोधन इस मामले में पूरी तरह से अनुपयुक्त हो गया।
- न्यायालय ने इसे एक सुस्थापित विधि माना कि 1956 से पहले मृत व्यक्तियों पर लागू मिताक्षरा विधि के अधीन, एक पुत्री अपने पिता की संपत्ति, चाहे वह पैतृक हो या स्व-अर्जित, उत्तराधिकार पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि ऐसी संपत्ति पूरी तरह से पुरुष संतान पर हस्तांतरित होती है, और केवल पुरुष संतान की अनुपस्थिति में ही पत्नी या पुत्री उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हिन्दू उत्तराधिकार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929 ने शास्त्रीय हिंदू विधि की मौलिक अवधारणाओं को संशोधित नहीं किया है या पिता की संपत्ति में पुत्र के पूर्ण अधिकार को प्रभावित नहीं किया है, अपितु केवल उत्तराधिकारियों के दायरे को बढ़ाया है, जो पुरुष संतान न होने पर कुछ महिला उत्तराधिकारियों को सम्मिलित करके उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यायालय ने अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर (2020) और अरुणाचल गौंडर बनाम पोन्नुसामी (2022) में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर व्यापक रूप से विश्वास किया, जिसमें कहा गया कि यदि उत्तराधिकार 1956 से पहले पुराने हिंदू विधि के अधीन खुलता है, तो पक्षकार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित होंगे, जिसमें लड़की केवल लड़के की अनुपस्थिति में ही अधिकार का दावा कर सकती है।
- न्यायालय ने निश्चित रूप से यह माना कि जब मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी हिंदू की मृत्यु 1956 से पहले हो जाती है, तो उसकी पृथक् संपत्ति पूरी तरह से उसके पुत्र को अंतरित हो जाती है, और तदनुसार, सुधीन की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पूरी तरह से बैगादास को हस्तांतरित हो जाती है, जिन्होंने सही ढंग से अपने अधिकारों को प्रतिवादियों को हस्तांतरित कर दिया।
- न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में नामांतरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई तथा यह माना कि संपत्ति विभाज्य नहीं है, जिससे वादी-अपीलकर्त्ता के विरुद्ध विधि के सभी तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तथा परिणामस्वरूप लागत के संबंध में कोई आदेश दिये बिना द्वितीय अपील को खारिज कर दिया गया।
मिताक्षरा विधि और पुत्रियों के उत्तराधिकार अधिकार के संबंध में क्या जानकारी दी गई?
- हिंदू विधि की मिताक्षरा स्कूल:
- मिताक्षरा विधि, प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों और स्मृतियों पर आधारित, 1956 से पहले उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली हिंदू विधि की प्राचीन पद्धति है।
- मिताक्षरा विधि के अधीन, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र जन्म के समय पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सहदायिकी अधिकार का निर्माण होता है।
- पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में अंश जन्म से ही मिलता है, पिता की मृत्यु या उत्तराधिकार से नहीं।
- जब कोई पुरुष अपने पूर्वजों से तीन डिग्री तक की संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, तो उसके तीन डिग्री नीचे तक के पुरुष उत्तराधिकारियों को स्वतः ही समान सहदायिकी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
- हिंदू उत्तराधिकार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929:
- 1929 का अधिनियम सबसे पहला सांविधिक विधायन था, जिसमें कुछ महिला उत्तराधिकारियों को सम्मिलित करके हिंदू महिलाओं को उत्तराधिकार योजना में सम्मिलित किया गया।
- 1929 के अधिनियम की धारा 1 केवल पुरुषों की उस संपत्ति पर लागू होती है जो सहदायिकी नहीं है और जिसका वसीयत द्वारा निपटान नहीं किया गया है।
- धारा 2 में पिता के पिता के बाद उत्तराधिकार क्रम में पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, बहन और बहन के पुत्र को सम्मिलित किया गया, किंतु पुत्रियों को पुत्रों के समान दर्जा नहीं दिया गया।
- धारा 3 में उपबंध है कि 1929 के अधिनियम के अधीन महिलाओं को मिताक्षरा विधि के अधीन महिलाओं के पास विद्यमान संपत्ति से अधिक संपत्ति नहीं दी जाएगी।
- 1929 के अधिनियम ने उत्तराधिकार के अधिकारों में कोई परिवर्तन किये बिना कुछ महिला उत्तराधिकारियों का वर्गीकरण 'बंधुओं' से बदलकर 'गोत्र सपिंडों' में कर दिया।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने हिंदुओं के बीच बिना वसीयत के उत्तराधिकार विधियों को संहिताबद्ध और सुधार कर क्रांतिकारी परिवर्तन लाया।
- धारा 8 ने पुरानी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जिसके अनुसार 1956 के बाद विरासत में मिली स्व-अर्जित संपत्ति सहदायिक संपत्ति नहीं बनती।
- 1956 का अधिनियम केवल इसके प्रारंभ होने के बाद आरंभ होने वाले उत्तराधिकारों पर लागू होता है, अर्थात् जहाँ मृतक की मृत्यु 17 जून 1956 को या उसके बाद हुई हो।
- धारा 6 को 2005 में संशोधित किया गया था, जिससे पुत्रियों को समान सहदायिकी अधिकार प्रदान किये गए, किंतु यह केवल भावी रूप से लागू होता है, 1956 से पूर्व के उत्तराधिकारियों पर नहीं।
- धारा 14 ने विधवाओं के सीमित हित को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया, किंतु यह केवल वहीं लागू होता है जहाँ विधवा अधिनियम के लागू होने के बाद भी जीवित रही हो।
- 1956 अधिनियम की प्रयोज्यता उत्तराधिकार खुलने के समय (मृत्यु की तिथि) पर निर्भर करती है, न कि अधिकारों का दावा करने या वाद दायर करने की तिथि पर।
- हिंदू महिला अधिकार और स्वामित्व अधिकार अधिनियम, 1937:
- 1937 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विधवाओं को पति की संपत्ति में केवल सीमित अधिकार दिया गया, पूर्ण स्वामित्व नहीं।
- यदि विधवा ने 1956 के बाद भी कब्जा जारी रखा तो धारा 14 के अधीन भूमिस्वामी के रूप में उसका सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है।
- 1956 से पहले और 1956 के बाद के कानून के बीच अंतर:
- 1956 से पहले के कानून के तहत पैतृक पुरुष पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्ति सहदायिक संपत्ति बनी रही, जिससे पुरुष वंशजों को अधिकार प्राप्त हुए।
- 1956 के बाद, पैतृक पूर्वजों से विरासत में प्राप्त स्व-अर्जित संपत्ति, सह-दायित्व वाली संपत्ति न होकर स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है।
- संपत्ति की प्रकृति और उत्तराधिकार के अधिकार उत्तराधिकार खुलने पर लागू कानून द्वारा निर्धारित होते हैं, न कि बाद में होने वाले विधायी परिवर्तनों द्वारा।
- विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के अधीन पुत्रियों के अधिकार:
- 1956 से पहले मिताक्षरा विधि के अधीन, यदि पुत्र जीवित हो तो पुत्री को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि संपत्ति केवल पुरुष के अंश में ही आती थी।
- पुत्री पिता की पृथक् संपत्ति का उत्तराधिकार केवल तभी प्राप्त कर सकती है जब कोई पुत्र न हो, उत्तराधिकार क्रम में उसका स्थान पाँचवाँ है।
- 1929 के अधिनियम के बाद भी, यदि पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो जाती थी तो पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे।
- पुत्रियों के अधिकारों को 1956 के बाद बढ़ाया गया तथा 2005 के संशोधन द्वारा और मजबूत किया गया, किंतु ये केवल संबंधित अधिनियमन तिथियों के बाद शुरू होने वाले उत्तराधिकारों पर ही लागू होते हैं।