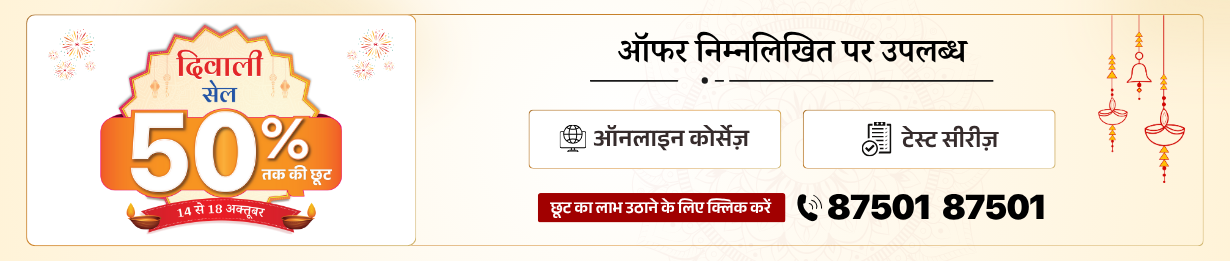करेंट अफेयर्स और संग्रह
होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह
सांविधानिक विधि
नैतिक (मोरल) पुलिसिंग और महिलाओं के सांविधानिक अधिकार
13-Oct-2025
|
नवनीता बनाम तमिलनाडु राज्य और ए अरुण कुमार न्यायालय ने कहा कि नैतिक पुलिसिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता की सांविधानिक गारंटी पर सीधा हमला है। न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी |
स्रोत: मद्रास उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
नवनिथा बनाम तमिलनाडु राज्य और ए. अरुण कुमार (2025) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी ने नैतिक पुलिसिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे और एक महिला की आत्महत्या से इसके सीधे संबंध को संबोधित किया, साथ ही इस तरह के आचरण को रोकने के लिये जमानत की शर्तों को मजबूत किया।
- इसमें आगे बताया गया कि महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर नैतिक पुलिसिंग की सबसे बुरी शिकार होती हैं और ऐसी नैतिक पुलिसिंग भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 21 के अधीन उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
नवनिथा बनाम तमिलनाडु राज्य और ए. अरुण कुमार (2025) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला चिन्नमनूर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 439/2024 से उत्पन्न हुआ ।
- याचिकाकर्ता की पुत्री की आत्महत्या के बाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संदिग्ध मृत्यु से संबंधित) की धारा 194(3) के अधीन मामला प्रारंभ में दर्ज किया गया था।
- अन्वेषण के दौरान पता चला कि अभियुक्त ए. अरुण कुमार ने मृतका के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जबकि वह अंदर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रही थी, जबकि उसका पति केरल में काम के लिये गया हुआ था।
- इस घटना से मृतका और उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के बीच अवैध संबंध की अफवाह फैल गई, जो पूरे गांव में फैल गई।
- इन अफवाहों के कारण सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण ग्रामीणों की नजरों में मृतक का अपमान और कलंक लगा।
- सामाजिक अपमान और बहिष्कार सहन न कर पाने के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली।
- पुलिस ने इस मामले में ए. अरुण कुमार और रामकुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
- ए. अरुण कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, लेकिन आठ दिनों के भीतर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।
- जमानत समय से पहले दिये जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए Crl.M.P.No. 542/2025 दायर किया।
- सेशन न्यायाधीश ने जमानत रद्द करने की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि कोई ठोस मामला नहीं बनता।
- वर्तमान पुनरीक्षण याचिका उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायपीठ ने नैतिक पुलिसिंग को एक खतरनाक और प्रतिगामी प्रथा बताते हुए इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसे कोई विधिक मंजूरी नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण समाज में महिलाएं इस तरह की निगरानी संबंधी गतिविधियों की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं।
- न्यायालय ने कहा कि नैतिक पुलिसिंग संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जो सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तथा सामाजिक बहिष्कार और दुखद परिणामों को बढ़ावा देता है।
- न्यायपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) और आईसीसीपीआर (ICCPR) के अधीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाए तो यह महिलाओं को उन सतर्कता कार्यों से बचाने का आदेश देता है जो उनकी गरिमा को धूमिल करते हैं और मौलिक अधिकारों से समझौता करते हैं।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अधीन अभियुक्तों के अधिकारों को नैतिक पुलिसिंग को रोकने में सामाजिक हित के साथ संतुलित किया।
- न्यायालय ने जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया, लेकिन नैतिक पुलिसिंग के विरुद्ध निवारक के रूप में जमानत की शर्तों को मजबूत कर दिया।
- आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को जमानत शर्तों में संशोधन के साथ निपटाया गया।
नैतिक पुलिसिंग क्या है?
- नैतिक पुलिसिंग से तात्पर्य स्वयंभू व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों पर नैतिकता और सामाजिक मानदंडों की अपनी धारणा को लागू करने की प्रथा से है।
- इसमें आमतौर पर सतर्कता संबंधी कार्यवाहियां शामिल होती हैं, जहां व्यक्ति स्वयं उस आचरण की निगरानी, नियंत्रण या दण्ड देने का कार्य करते हैं, जिसे वे अनैतिक या सामाजिक रूप से अनुचित मानते हैं।
- नैतिक पुलिसिंग अक्सर महिलाओं को निशाना बनाती है, विशेष रूप से ग्रामीण और पारंपरिक समुदायों में, तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करती है।
- इस तरह की कार्रवाइयों को कोई विधिक मंजूरी नहीं मिलती है और ये सामाजिक नैतिकता की व्यक्तिपरक व्याख्याओं से प्रेरित होती हैं।
- नैतिक पुलिसिंग के परिणामस्वरूप अक्सर पीड़ितों को सामाजिक बहिष्कार, उत्पीड़न और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है।
- गंभीर मामलों में, जैसा कि इस निर्णय में प्रमाणित है, नैतिक पुलिसिंग ने पीड़ितों को आत्महत्या सहित दुखद परिणामों की ओर धकेला है।
- ग्रामीण समुदायों में नैतिक पुलिसिंग के कारण महिलाओं के विरुद्ध सम्मान के नाम पर हत्याएं, जबरन विवाह, आत्महत्याएं और अन्य प्रकार की हिंसा हुई है।
भारतीय संविधान (COI) का अनुच्छेद 21 क्या है?
बारे में:
- अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है । इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू भी शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार सुरक्षित करता है:
- जीवन का अधिकार
- वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार
- इस अनुच्छेद को जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण करने वाला प्रक्रियात्मक मैग्ना कार्टा कहा गया है।
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है ।
- यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद 21 के अधीन अधिकार:
- अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं :
- निजता का अधिकार
- विदेश जाने का अधिकार
- आश्रय का अधिकार
- एकांत परिरोध या कारावास के विरुद्ध अधिकार
- सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार
- हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
- अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार
- विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार
- डॉक्टरों की सहायता पाने का अधिकार
- सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार
- प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास का अधिकार
- स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा
वाद विधि:
- फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक (1981) के मामले में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने कहा था कि सांविधानिक दायित्व संहिता का अनुच्छेद 21 एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व के सांविधानिक मूल्य को समाहित करता है।
- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन शब्द का तात्पर्य केवल पशुवत अस्तित्व से कहीं अधिक है। इससे वंचित होने का निषेध उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। यह प्रावधान शरीर के किसी कवचयुक्त पैर को काटकर या आँख निकालकर, या शरीर के किसी अन्य अंग को नष्ट करके शरीर को विकृत करने पर भी समान रूप से प्रतिबंध लगाता है जिसके माध्यम से आत्मा बाहरी दुनिया से संपर्क करती है।
सांविधानिक विधि
धर्म का पालन करने का अधिकार
13-Oct-2025
|
मोहम्मद तैय्यब बनाम मध्य प्रदेश राज्य "हमारा सुविचारित मत है कि रिट न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करके सही किया है। याचिकाकर्त्ताओं का मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।" न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी |
स्रोत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने उज्जैन की तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 25 के अधीन धार्मिक आचरण का अधिकार किसी विशिष्ट स्थान से बंधा नहीं है। 1978 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि मस्जिद वाली भूमि का अधिग्रहण धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहम्मद तैय्यब बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
मोहम्मद तैय्यब बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- अपीलकर्त्ता, मोहम्मद तैय्यब और अन्य, उज्जैन के स्थानीय निवासी हैं, जो नियमित रूप से राजस्व मंडल-3, तहसील उज्जैन के सर्वेक्षण क्रमांक 2324-2329 पर स्थित तकिया मस्जिद में नमाज अदा करते थे।
- मस्जिद की स्थापना लगभग 200 वर्ष पहले हुई थी और इसे 13 दिसंबर, 1985 की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था।
- राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकाल लोक परिषद के पार्किंग स्थल के विस्तार के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है।
- राज्य ने एक निर्णय पारित किया, अतिक्रमणकारी बताए गए व्यक्तियों को प्रतिकर वितरित किया और 11 जनवरी, 2025 को मस्जिद को ध्वस्त कर दिया।
- अपीलकर्त्ताओं ने रिट याचिका संख्या 1515/2025 दायर कर मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिये निदेश देने और उत्तरदायी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू करने की मांग की।
- राज्य ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किया गया था तथा सभी संपत्तियां राज्य सरकार के पास थीं।
- राज्य ने आगे तर्क दिया कि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दायर कई रिट याचिकाएँ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं।
- मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83(2) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण के समक्ष एक सिविल वाद दायर किया था, जिसमें मालिकाना हक और प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार का दावा किया गया था।
- एकल न्यायाधीश ने 4 सितंबर, 2025 के आदेश के अधीन रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिग्रहण की कार्यवाही अंतिम चरण में पहुँच चुकी है।
- अपीलकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती देते हुए रिट अपील संख्या 2782/2025 दायर की।
- अपीलकर्त्ताओं ने गुरुवायूर देवस्वोम प्रबंध समिति मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भक्त होने के नाते उन्हें पुनर्निर्माण की मांग करने का अधिकार है।
- अपीलकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अधीन प्रदत्त उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- अपीलकर्त्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि एक बार जब संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो वह सदैव के लिये वक्फ संपत्ति ही रहती है और इसलिये इसे सदोष तरीके से अर्जित किया गया है।
- राज्य ने मोहम्मद अली खान मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्त्ताओं के पास याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि मस्जिद और भूमि का अधिग्रहण विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन किया गया था तथा भूमि पर कब्जा रखने वाले अनेक व्यक्तियों को प्रतिकर वितरित किया गया था।
- न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अपीलकर्त्ता अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दे रहे थे, लेकिन वे अनुतोष खण्ड में इसे रद्द करने की मांग नहीं कर रहे थे।
- न्यायालय ने कहा कि अधिग्रहण कार्यवाही और पंचाट को रद्द करने के लिये अनुतोष मांगे बिना, पुनर्स्थापन और परिणामी निर्माण का अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकता।
- न्यायालय ने धर्म के पालन के अधिकार के संबंध में मोहम्मद अली खान मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्ण सहमति व्यक्त की।
- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत धर्म का पालन, आचरण और प्रचार एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसका किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मस्जिद में, अपने घर में या अन्यत्र नमाज अदा कर सकता है, तथा वह किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि जिस भूमि पर मस्जिद है, उसका अधिग्रहण किसी व्यक्ति को उसके धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं माना जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 31 के अधीन है, तथा अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत स्वतंत्रता राज्य के वैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को नहीं छीन सकती।
- न्यायालय ने कहा कि धर्म का पालन करने के अधिकार में कहीं भी इसका पालन करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है, न कि किसी विशेष स्थान पर इसका पालन करने की स्वतंत्रता।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्त्ताओं को मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।
- न्यायालय को रिट याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
- न्यायालय ने लागत के संबंध में कोई आदेश दिये बिना रिट अपील को खारिज कर दिया।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रदत्त अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा और महत्त्व क्या है?
- भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं, और अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत स्वतंत्रता भाग 3 में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन है।
- अनुच्छेद 25 - अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता।
- खण्ड (1) - सामान्य अधिकार:
- अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है।
- अनुच्छेद 25(1) के अधीन स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन है।
- अनुच्छेद 25(1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकार सभी व्यक्तियों को उनकी धार्मिक संबद्धता के होते हुए भी समान अधिकार सुनिश्चित करता है।
- खण्ड (2) - विनियमन करने की राज्य की शक्ति:
- अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिये विधि बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 25(2) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये और लोक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिये खोलने हेतु विधि बनाने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 25 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी विद्यमान विधि के संचालन को प्रभावित करे या राज्य को नियामक विधि बनाने से रोके।
- स्पष्टीकरण:
- स्पष्टीकरण 1 में यह उपबंधित किया गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण 2 में यह उपबंधित है कि हिंदुओं और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति और उनकी संबंधित धार्मिक संस्थाएँ सम्मिलित होंगी।
- निर्वचनात्मक सिद्धांत:
- धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषित करने का अधिकार।
- धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता में अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार कार्य करने और धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार सम्मिलित है।
- धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता में अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक संप्रेषित करने और फैलाने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अनुच्छेद 26 के अधीन सामूहिक या संस्थागत अधिकारों से भिन्न व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 25 के अधीन स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसका किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से कोई आवश्यक संबंध नहीं है जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है।
सिविल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21
13-Oct-2025
|
संतोष पात्रा बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य "सिविल विधि में यह अत्यंत मौलिक है कि, पूर्व-न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते... क्योंकि, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश-21, जिसमें डिक्री और आदेशों के निष्पादन हेतु कुल 106 नियम सम्मिलित हैं, एक स्व-निहित और स्वतंत्र आदेश है। इसलिये, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में उपलब्ध पूर्व-न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते।" न्यायमूर्ति आनंद चंद्र बेहरा |
स्रोत: उड़ीसा उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति आनंद चंद्र बेहरा ने यह निर्णय दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 11 के अधीन पूर्व-न्याय का सिद्धांत आदेश 21 के अधीन निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र संहिता है, जो तकनीकी दोषों के होते हुए भी डिक्रीदारों को नए निष्पादन आवेदन दायर करने की अनुमति देता है।
- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने संतोष पात्रा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
संतोष पात्रा बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- याचिकाकर्त्ता, संतोष पात्रा, 1987 के मनी सूट संख्या 76 में मूल डिक्रीदार (DHR) थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके पक्ष में निर्णय और डिक्री हुई थी।
- उक्त डिक्री के अनुसरण में, याचिकाकर्त्ता ने सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), सोनपुर के समक्ष निष्पादन वाद संख्या 04/1991 स्थापित किया, जिसमें मनी सूट संख्या 76/1987 में पारित डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई।
- याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर की गई निष्पादन याचिका में निर्णीतऋणी (JDR) से कुछ राशि और संपत्तियों की वसूली की मांग की गई थी, जिसमें दो सरकारी वाहनों के रूप में चल संपत्तियाँ और निष्पादन आवेदन से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित अचल संपत्तियाँ सम्मिलित थीं।
- विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), सोनपुर ने दिनांक 27.09.2024 के आदेश के अधीन तकनीकी आधार पर निष्पादन वाद संख्या 04/1991 को खारिज कर दिया।
- निष्पादन याचिका को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि यह कई कमियों के कारण निष्पादन योग्य नहीं थी, अर्थात् डिक्रीदार निर्णीतऋणीओं से वसूल की जाने वाली धनराशि की सही राशि को इंगित करने में असफल रहा था; दो सरकारी वाहनों का कोई मूल्यांकन प्रदान नहीं किया गया था; और अनुसूची में उल्लिखित अचल संपत्तियों का कोई मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- दिनांक 27.09.2024 के विवादित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्त्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें निष्पादन मामले को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि तकनीकी त्रुटियों को सुधारने और विधि के अधीन अपेक्षित विवरण प्रदान करने का अवसर दिये बिना निष्पादन मामले को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये था।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि यह सिविल विधि का एक मौलिक सिद्धांत है कि पूर्व-न्याय' का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।
- न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21, जिसमें डिक्री और आदेशों के निष्पादन के लिये कुल 106 नियम हैं, एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आदेश है।
- आदेश 21 एक स्व-निहित संहिता होने के कारण, न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में निहित पूर्व-न्याय के सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी तकनीकी आधार पर निष्पादन कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया जाता है, वहाँ निर्णीतऋणी को निष्पादन याचिका को निष्पादन योग्य बनाने के लिये सही विवरण प्रदान करके निष्पादन के लिये नया आवेदन दायर करने से विधि के अधीन रोका नहीं जाता है।
- न्यायालय ने कहा कि किसी डिक्रीदार (DHR) को केवल निष्पादन के लिये आवेदन में तकनीकी त्रुटियों, जैसे चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करने के कारण डिक्री का फल प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय ने कहा कि विधि के अनुसार, न्यायालय द्वारा डिक्रीदार को निष्पादन के लिये आवेदन में आवश्यक विवरण देने का अवसर दिया जाना आवश्यक है जिससे उसमें विद्यमान दोषों को दूर किया जा सके।
- न्यायालय ने पाया कि विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), सोनपुर ने निष्पादन आवेदन में दर्शाई गई संपत्तियों के अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के लिये याचिकाकर्त्ता को कोई अवसर प्रदान किये बिना ही निष्पादन वाद संख्या 04/1991 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया था।
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 11, उपखण्ड (2) और परिशिष्ट (E) संख्या 6 के उपबंधों का पालन करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो निष्पादन के लिये विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता को ऐसा अवसर प्रदान न किये जाने के कारण, 27.09.2024 का आदेश विधि के अधीन कायम नहीं रह सकता।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अस्वीकार करना, विधि के अधीन कोई औचित्य नहीं है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21 क्या है?
- आदेश 21 का शीर्षक "डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन" है और यह न्यायालय के आदेशों और डिक्रियों के निष्पादन को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक संहिता है।
- आदेश 21 में कुल 106 नियम हैं, जो इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आदेश बनाता है।
- आदेश में डिक्री के अधीन धन संदाय की विभिन्न रीतियों का उपबंध है, जिसमें न्यायालय के अंदर और बाहर संदाय भी सम्मिलित है।
- यह डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालयों की अधिकारिता को विहित करता है, जिसमें अन्य अधिकारिता वाले न्यायालयों और लघु वाद न्यायालयों को निष्पादन अंतरित करने के उपबंध भी सम्मिलित हैं।
- आदेश में मौखिक और लिखित आवेदनों सहित निष्पादन के लिये आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, तथा गिरफ्तारी, चल संपत्ति की कुर्की और अचल संपत्ति की कुर्की की मांग करने वाले आवेदनों के लिये आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।
- इसमें निष्पादन के लिये प्रक्रिया जारी करने तथा उन परिस्थितियों का उपबंध है जिनके अधीन न्यायालय डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा सकते हैं।
- आदेश 21 में डिक्री की प्रकृति के आधार पर निष्पादन की विभिन्न रीतियों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें धन के संदाय, विशिष्ट चल या अचल संपत्ति का परिदान, विनिर्दिष्ट पालन, वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यास्थापन, व्यादेश और दस्तावेज़ों के निष्पादन के लिये डिक्री सम्मिलित हैं।
- आदेश में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की कुर्की के संबंध में विस्तृत उपबंध हैं, जिनमें चल संपत्ति, कृषि उपज, ऋण, अंश, वेतन और भत्ते, भागीदारी संपत्ति, परक्राम्य लिखत और अचल संपत्ति सम्मिलित हैं।
- इसमें पर-पक्षकार द्वारा संपत्ति की कुर्की के दावों और आपत्तियों के न्यायनिर्णयन का उपबंध है।
- आदेश 21 में कुर्क की गई चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के विक्रय से संबंधित व्यापक उपबंध सम्मिलित हैं, जिनमें उद्घोषणा की आवश्यकताएँ, विक्रय का संचालन, क्रेता के अधिकार और विभिन्न आधारों पर विक्रय को अपास्त करना सम्मिलित है।
- आदेश में डिक्रीदारों या क्रेताओं को संपत्ति के कब्जे की सुपर्दगी तथा प्रतिरोध, अवरोध या बेदखली के मामलों में उपचार का उपबंध है।
- इसमें प्रक्रियागत मामलों के लिये उपबंध सम्मिलित हैं, जैसे विक्रय का स्थगन या रोक, कुछ व्यक्तियों द्वारा बोली लगाने पर प्रतिबंध, तथा कुछ नियमों के अधीन पारित आदेशों को डिक्री के रूप में मानना।